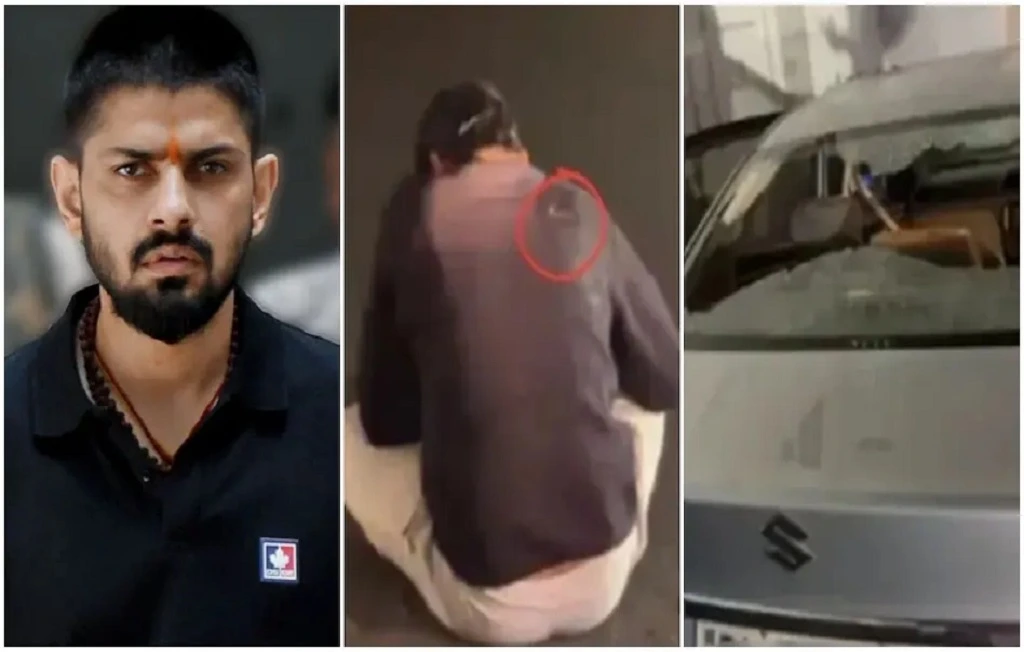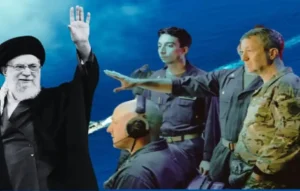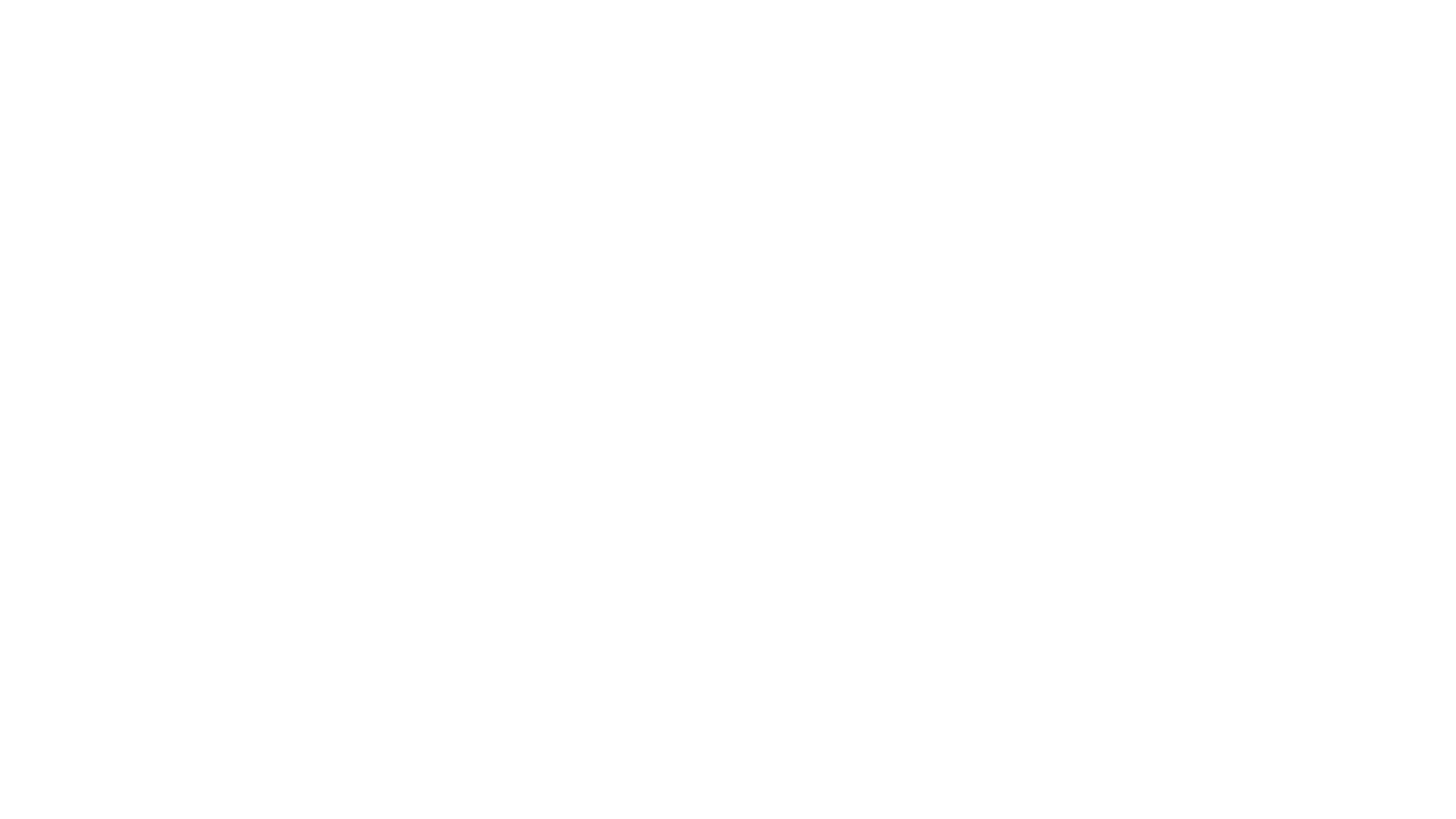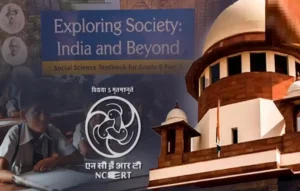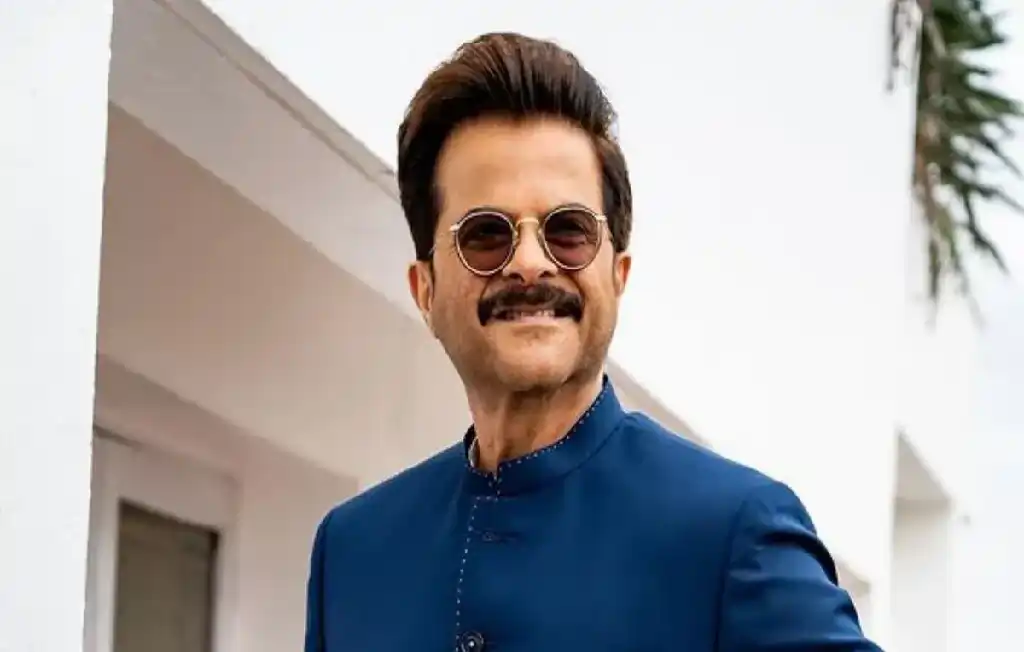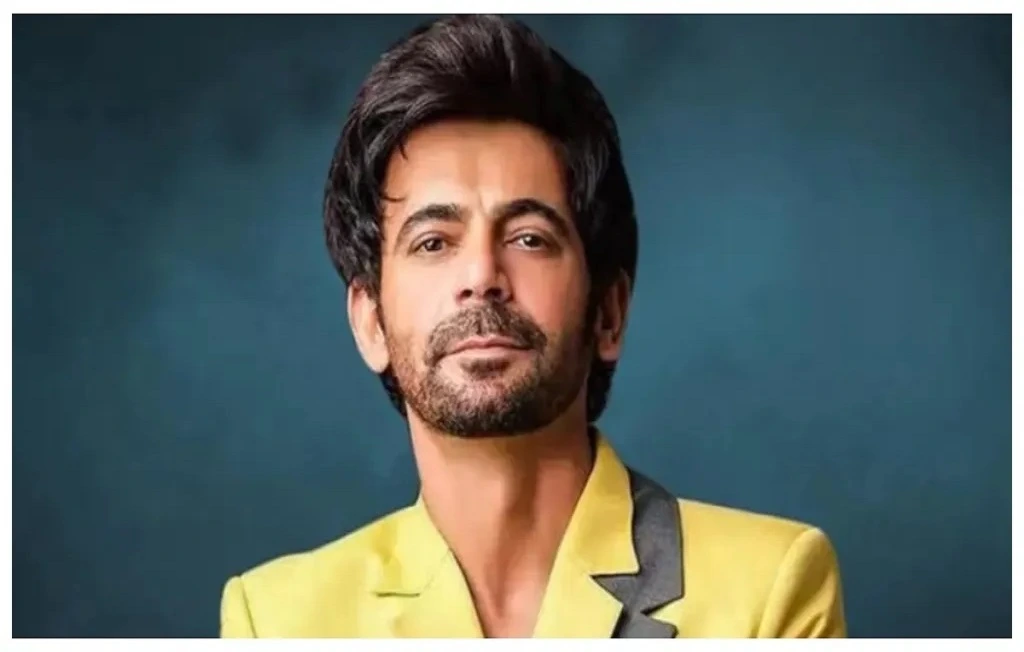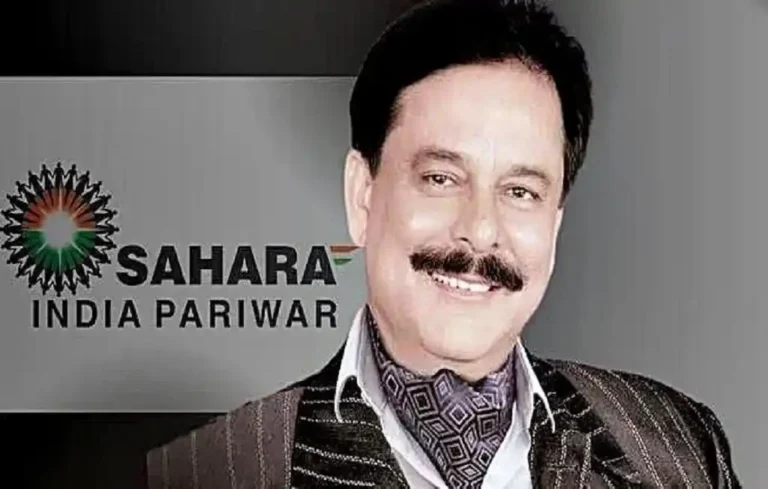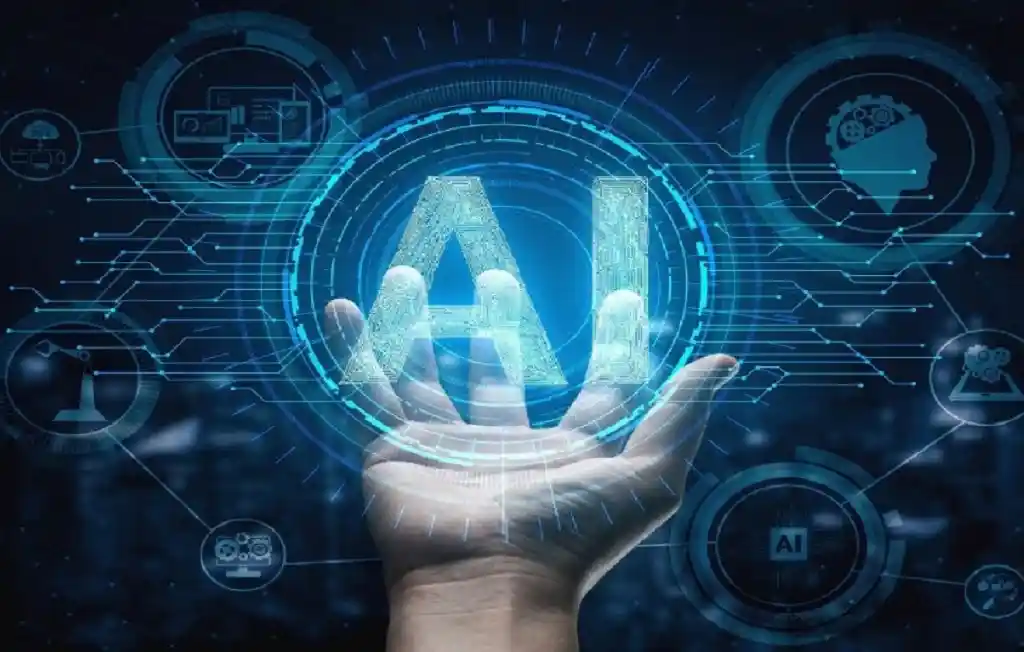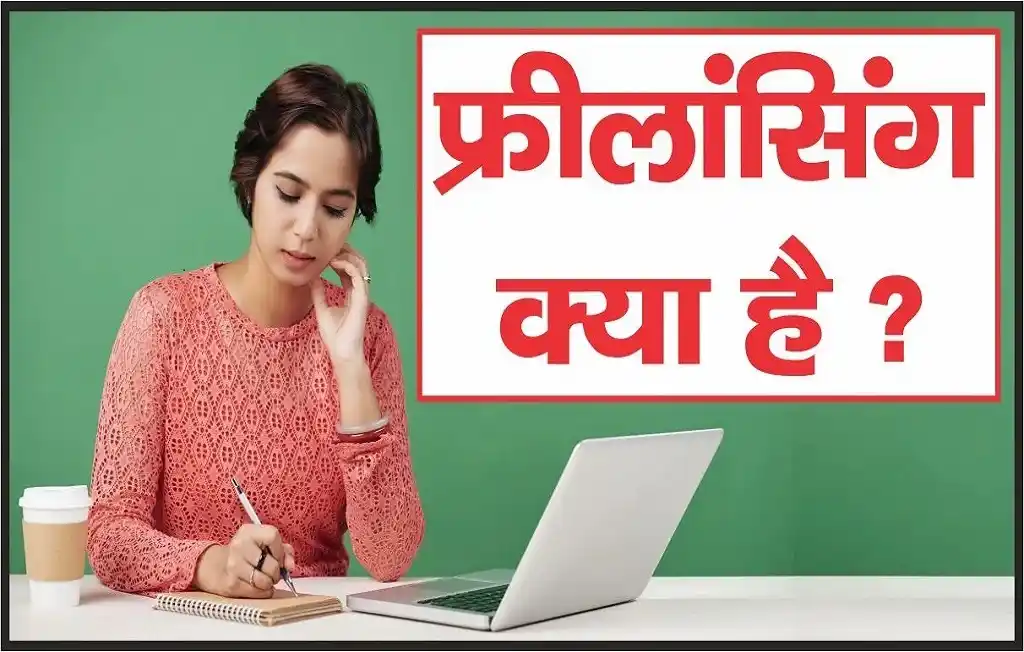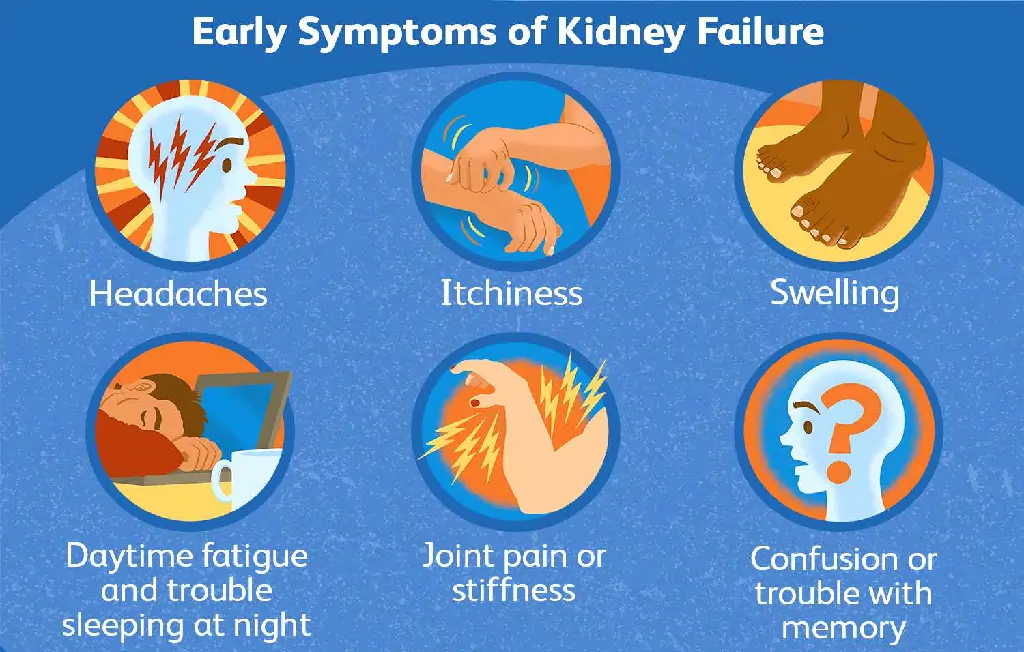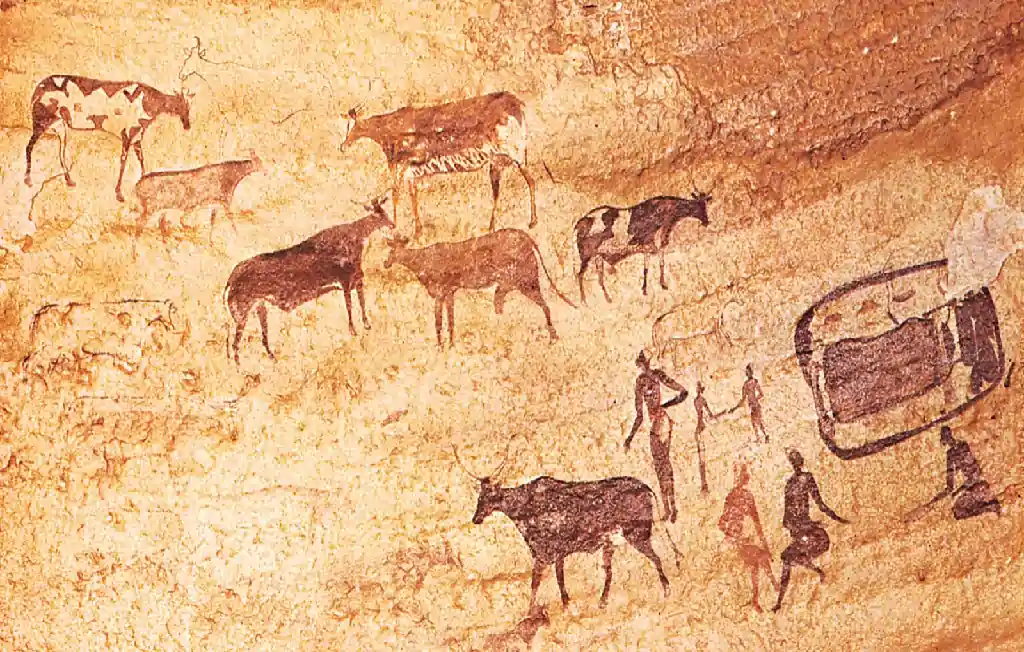/ Feb 28, 2026
Trending